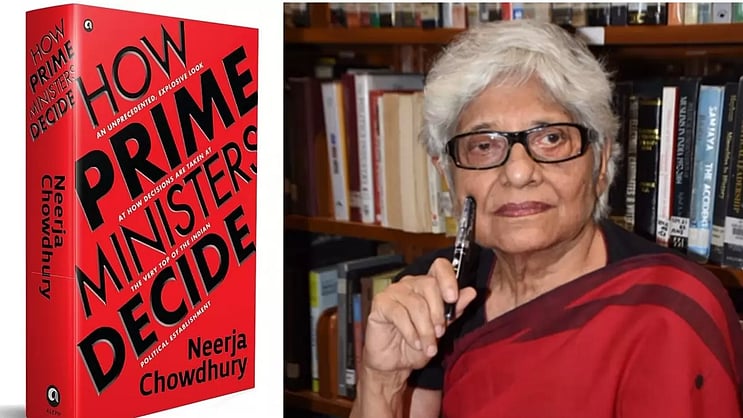समाचार मंच
इस समय देश की न्यायपालिका और विधायिका के बीच ‘तलवारें‘ खिंची नजर आ रही है।न्यायपालिका जो कई संवैधानिक संस्थाओं को पिंजरे का तोता बताती रही है,कभी-कभी लगता है कि उसकी भी स्थिति कहीं कुछ वैसी ही तो नहीं है। यह हद ही है कि न्यायपालिका महामहिम राष्टपति को निर्देश देती है,संसद से पास कानून की अपने हिसाब से व्याख्या करती है। इतना ही नहीं वह सामने वाले की हैसियत देखकर यह निर्णय तक लेती है कि कौन सा केस कब सुना या नहीं सुना जायेगा।वक्फ बोर्ड कानून में किये गये परिर्वतन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट यही कर रही है। जबकि संविधान में सबकी मर्यादा तय है। देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने इन संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की व्यवस्था की थी, ताकि कोई एक संस्था अत्यधिक प्रभावशाली न बन जाए। लेकिन समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला है, जो इस शक्ति-संतुलन को परखने वाला साबित हुआ है। यह टकराव अक्सर नीतिगत फैसलों, विधायी संशोधनों और अधिकारों की व्याख्या को लेकर हुआ है।
भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहला बड़ा टकराव संसद और न्यायपालिका के बीच श्गोला केसश् के रूप में सामने आया, जिसमें भूमि सुधारों को लेकर संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई थी। सरकार ने भूमि सुधारों को सामाजिक न्याय का हिस्सा मानते हुए कानून बनाए, परंतु अदालत ने इन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया। इसके बाद संविधान में कई संशोधन किए गए, खासकर पहला और चैथा संशोधन, ताकि संसद को अधिक अधिकार मिल सकें। लेकिन इस टकराव की पराकाष्ठा 1973 में श्केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यश् केस में देखने को मिली, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की श्मूल संरचनाश् को नहीं बदल सकती। इस निर्णय ने संसद की शक्ति को सीमित कर दिया और न्यायपालिका को संविधान का अंतिम व्याख्याकार घोषित किया।
इसके बाद इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया, तो इसके प्रतिउत्तर में तत्कालीन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की और 42वां संविधान संशोधन लाकर न्यायपालिका की शक्ति सीमित करने की कोशिश की। इस संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और मूल संरचना सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इस संशोधन के कुछ हिस्सों को 44वें संशोधन द्वारा वापस लिया गया। यह घटनाक्रम सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सबसे बड़े संघर्षों में गिना जाता है।
सहाबानो केस एक ऐतिहासिक और विवादास्पद मामला था, जिसने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। यह मामला 1978 में शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश की रहने वाली 62 वर्षीय मुस्लिम महिला सहाबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 40 साल की शादी के बाद तलाक दे दिया। सहाबानो ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर कर अपने भरण-पोषण के लिए गुजारा भत्ता (उंपदजमदंदबम) की मांग की थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत दी जाती है।
निचली अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया, जिसे उनके पति ने यह कहकर चुनौती दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के बाद पत्नी केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण-पोषण की हकदार होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सहाबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि धारा 125 धर्म से ऊपर है और सभी महिलाओं को समान अधिकार है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद उचित भरण-पोषण मिलना चाहिए।
इस फैसले के बाद देशभर में विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने इसे धार्मिक हस्तक्षेप माना। इसके जवाब में 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण के अधिकार) अधिनियम पारित किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावहीन हो गया।
1990 के दशक में एक और बड़ा टकराव हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने श्एस आर बोंसलेश् केस में आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की सीमा 50ः से अधिक नहीं हो सकती। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का रास्ता खोल दिया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं थी और संविधान संशोधन के माध्यम से अपने अधिकारों का विस्तार करना चाहती थी।
1993 में दूसरा बड़ा टकराव उस समय सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने श्विरोधी नियुक्तियोंश् पर सरकार की भूमिका को सीमित करते हुए श्कॉलेजियम सिस्टमश् को लागू किया। यह व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका से स्वतंत्र मानी गई, लेकिन सरकार को यह प्रणाली कभी रास नहीं आई। समय बीतने के साथ इस प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे और 2014 में केंद्र सरकार ने श्राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगश् (छश्र।ब्) कानून बनाया, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करना और एक अधिक संतुलित प्रणाली लाना था जिसमें सरकार की भी भागीदारी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा। यह निर्णय सरकार के लिए एक बड़ा झटका था और इसके बाद से न्यायपालिका की नियुक्ति को लेकर दोनों संस्थाओं के बीच तनातनी बनी रही।
हाल ही में 2023-24 के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिला जब कॉलेजियम की सिफारिशों को लेकर सरकार ने नियुक्तियों में देरी की या उन्हें लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और सरकार को फटकार लगाई कि वह संविधान सम्मत प्रक्रिया का पालन करे। एक और बड़ा मुद्दा दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण निर्वाचित सरकार के पास होना चाहिए, न कि उपराज्यपाल के पास। केंद्र सरकार ने इस निर्णय के तुरंत बाद अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी कर दिया, जिसे बाद में कानून के रूप में पारित किया गया। यह घटनाक्रम न्यायपालिका की निर्णयात्मक शक्ति और कार्यपालिका की विधायी शक्ति के बीच सीधी टकराव का उदाहरण बना।
इसके अलावा, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप किया है जिन्हें सरकार नीतिगत मानकर न्यायिक समीक्षा के बाहर रखना चाहती थी। जैसे नोटबंदी, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, कृषि कानून आदि। इन मामलों में कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की लेकिन यह टकराव की संभावनाओं को खत्म नहीं कर सका।
अक्सर यह देखा गया है कि जब भी सरकार न्यायपालिका के दायरे में हस्तक्षेप करती है या न्यायपालिका सरकार की नीतियों की समीक्षा करती है, तब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और कार्यपालिका उससे प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन व्यवहार में यह सीमा अक्सर धुंधली हो जाती है।
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भारत में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं, बल्कि समय-समय पर उनमें वैचारिक, संवैधानिक और व्यावहारिक टकराव होता रहा है। यह टकराव हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और एक-दूसरे की शक्तियों की समीक्षा करने में सक्षम हैं। लेकिन जब यह टकराव अत्यधिक हो जाता है, या राजनीतिक रंग ले लेता है, तब लोकतांत्रिक संतुलन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों संस्थाएँ एक-दूसरे की संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करें और जनता के हित को सर्वोपरि मानें।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव की घटनाएँ न केवल भारतीय लोकतंत्र के विकास की कहानी कहती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि किस तरह संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन समय के साथ बदलता है और किस तरह न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में अहम होती है। यदि यह टकराव संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहे, तो यह व्यवस्था को सशक्त और उत्तरदायी बनाता है, लेकिन यदि यह संघर्ष सत्ता की लालसा और अधिकारों की होड़ में बदल जाए, तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। इसलिए, इस संतुलन को बनाए रखना ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और खूबसूरती दोनों है।